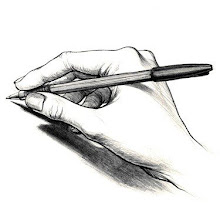भारतीय जनता पार्टी की तेजतर्रार नेता साध्वी उमा भारती 2005 में पार्टी से अचानक बाहर हो गई थीं। तब उनके निष्कासन को राजनीति विश्लेषक पार्टी की अंदरूनी खींच-तान का परिणाम मान रहे थे। इसके बाद 30 अप्रैल 2006 को उमा भारती ने उज्जैन के निकट स्थित महाकाल में नई पार्टी की घोषणा की। नाम रखा- भारतीय जनशक्ति पार्टी। उस समय अपनी पार्टी को भाजपा का पुनर्जन्म बताते हुए उमा ने खुद को 'पन्ना धाय' की संज्ञा दी थी और राष्ट्रवादी विचारधारा को जीवित रखने की प्रतिज्ञा ली थी। पर, लोकप्रियता के बावजूद उनकी पार्टी को मध्य प्रदेश में कोई खास चुनावी सफलता नहीं मिली। हालांकि, इस दौरान उमा भारती गंगा अभियान से भी जुड़ी रहीं। आखिरकार 25 मार्च, 2010 को उन्होंने अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और अब सात जून को भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अचानक उनके पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। उमा भारती बताती हैं कि यह अचानक क्यों हुआ, इसकी जानकारी तो उन्हें भी नहीं है। भावी योजनाओं के साथ-साथ इस बाबत प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के संपादित अंश। श्रुति अवस्थी और ब्रजेश कुमार से हुई पूरी बातचीत के लिए प्रथम प्रवक्ता पढ़ें।
सवाल: करीब छह साल बाद भारतीय जनता पार्टी में वापसी पर क्या महसूस कर रही हैं ?जवाब: छह साल नहीं, साढ़े पांच साल बाद। छह साल तो पूरे नहीं हुए। फिलहाल कुछ भी नया महसूस नहीं कर रही हूं, क्योंकि जब मैंने अलग पार्टी बनाई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और विचारधारा भी वही थी। यही वजह है कि भाजपा से जाना तो महसूस हुआ, पर आना महसूस नहीं हुआ। जब पार्टी से जाना हुआ तो संवाद में दूरी आ गई थी। इससे जाना महसूस हुआ, लेकिन अब जब आ गई हूं तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कोई चीज हुई हो।
सवाल: आपके पार्टी में लाए जाने की मीडिया में कई बार खबरें आईं, पर तब ऐसा नहीं हुआ। सात जून को अचानक इसकी घोषणा की गई। इसकी कोई खास वजह थी ?जवाब: इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हां, नितिन गडकरी जी और आडवाणी जी पिछले एक-डेढ़ साल से मुझे पार्टी में आने के लिए कह रहे थे। बाकि अचानक यह घटनाक्रम क्यों हुआ, यह मेरी जानकारी में नहीं है।
सवाल: आपके पार्टी में आने को इतना गोपनीय रखा गया कि यह खबर आई कि इसकी जानकारी खुद आपको भी नहीं थी कि सात जून को आप भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। इसकी कोई खास वचह तो होगी।जवाब: मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। आडवाणी जी, नितिन गडकरी जी और अशोक सिंघल जी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। मैं इन लोगों से किसी न किसी कारण लगातार संपर्क में रही हूं। वे लोग जो कुछ कह रहे हैं, वह सही है। मैं उनके निर्णय को ठीक मानती हूं।
सवाल: उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मांग पर आपको पार्टी में लाया गया। ऐसा कहा जा रहा है।जवाब: मैं देशभर में जहां भी जाती थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुझसे मिलते थे। वे पार्टी में आने का आमंत्रण देते थे। मैं गत दिसंबर के महीने में जब द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर गई थी तो वहां मंदिरों में श्रद्धालुओं का जो भी समूह मिलता था, वह एक ही बात कहता था कि आप भाजपा में शामिल हो जाइये। इसलिए मैं तो यही मानती हूं कि उत्तर प्रदेश ही क्यों, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता जहां भी होगा उसको इस बात से खुशी होगी कि मैं पार्टी में वापस आई हूं।
सवाल: पार्टी अध्यक्ष ने मुख्य तौर पर आपको जो जिम्मेदारी सौंपी है वह क्या है?जवाब: उन्होंने इसकी घोषणा की है। हां, मैं गंगा से जुड़े मुद्दे को लेकर पहले से सक्रिय थी और भाजपा में भी गंगा सेल है तो मुझे उसका काम सौंपा गया है।
सवाल: उत्तर प्रदेश में जगह-जगह से खबरें आ रही हैं कि आपकी भाजपा में वापसी से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। आपके शुक्रताल तीर्थ स्थल और मेरठ के कार्यक्रर्मों से भी यह स्पष्ट हुआ। तो क्या यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को उसका स्वाभाविक नेता मिल गया है ?जवाब: यह कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। हां, मैं यह जरूर मानती हूं कि मेरे आने से वे काफी खुश हैं। मैं पार्टी से चली गई थी तो इसका उन्हें दुख था। ऐसा बिलकुल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई नया नेता आ गया है। यहां नेताओं का अभाव नहीं है।
सवाल: यह सब 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, ऐसी धारणा है। आपके सामने दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस की ओर से यहां उपस्थित हैं। आप इस चुनौती को किस तरह देखती हैं? जवाब: मैं व्यक्तिगत स्तर पर कभी टकराव नहीं करती। न ही व्यक्तिगत स्तर पर हमारा किसी से विरोध है। दिग्विजय सिंह मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वे भी मुझे छोटी बहन मानते हैं। लेकिन हां, यह एक बड़ी नियती ही है कि मध्यप्रदेश में उन्हें हराने का काम मुझे मिला। इतना ही नहीं, मैं जब बिहार का काम देख रही थी तो चुनाव के दौरान वे लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस गठबंधन का जिम्मा संभाले हुए थे और लालू के वकील की भूमिका में थे। 2003 में मध्य प्रदेश में मेरे हाथों हारने के बाद वे बिहार में भी हारे। यह अजीब बात है कि उनको मात देने का मौका मुझे ही मिलता है।
सवाल: समय बदल गया है। 2003 में दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश तक सीमित थे। अब आठ साल बाद वे पार्टी के महासचिव और 10 जनपथ के वास्तविक प्रवक्ता के रूप में एक राष्ट्रीय नेता की छवि पा चुके हैं। इससे आपका काम कितना कठिन होगा ?उत्तर: मैंने आपसे पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वहां कांग्रेस तो सामने आए। हां, वहां हमें सपा और बसपा का मुकाबला करना है। कांग्रेस पार्टी वहां इतिहास का विषय बन गई है, इसलिए मैं नहीं मानती कि कांग्रेस से हमारी कोई टक्कर है।
सवाल: यही सही, पर सपा-बसपा से टक्कर के लिए ही पार्टी से आपको कितना सहयोग मिलेगा ?जवाब- मुझे पार्टी से सहयोग नहीं चाहिए। मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता हूं और इससे उलट यह मानती हूं कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि हम उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति को सुधारें, क्योंकि उत्तरप्रदेश से ही भारत की राजनीति में विकृतियां उत्पन्न हुई हैं। इस प्रदेश से दो प्रकार की राजनीति सामने आई। एक तो यह कि दलित वर्ग को यहां अपने दम पर सत्ता मिली। हालांकि, सबसे बड़ा दलित आंदोलन तमिलनाडु में हुआ। महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी आंदोलन चलाया। इसके बावजूद राजनीतिक आंदोलन के द्वारा सत्ता-शीर्ष तो उसे उत्तर प्रदेश में ही मिला, जब मायावती बहुमत प्राप्त कर मुख्यमंत्री बनीं।
पर यहां सबसे बुरी बात यह रही कि जो लोग मुसलमानों के हितैषी बनते थे, उन्हीं के शासनकाल में मुसलमानों की स्थिति दयनीय हुई। डॉन-माफियाओं के साथ जुड़ाव यहीं के मुसलमानों का माना गया। प्रदेश के बुनकर-जुलाहे निरंतर बेरोजगार होते गए। कुल मिलाकर आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सबसे खराब हालत है। अत: मैं मानती हूं कि राष्ट्रीय हितों को यदि साधना है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन लाना होगा। प्रदेश में वैचारिक धरातल पर जो आंदोलन चलते रहे हैं, उसके मूल तत्व को बाहर लाना होगा। मैं यह कदापि नहीं कह रही हूं कि उन आंदोलनों को नकारा जाए। मेरा इतना भर कहना है कि चाहे वह दलित आंदोलन हो या रामजन्म भूमि का आंदोलन, इन आंदोलनों के मूल तत्वों को निकालकर एक नए राजनैतिक आधार पर वहां सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी।
सवाल: ऐसे में उत्तर प्रदेश का चुनावी मुद्दा क्या होगा ? जवाब: ‘राम’ और ‘रोटी’ दोनों मुद्दा होगा। यानी मंडल भी और कमंडल भी। जो सांस्कृतिक आंदोलन हुए हैं, वह ‘कमंडल’ है और जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं वह ‘मंडल’ है। ‘राम-मंदिर से राम-राज्य की ओर’ यही हमारा मुख्य नारा होगा।
सवाल: लेकिन, पिछले दिनों मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल तीर्थ स्थल में तो आपने एक नया नारा दे दिया है।जवाब: आप ठीक कह रहे हैं। पर वहां मैंने कार्यकर्ताओं के बीच नारा दिया है। आम लोगों के बीच तो हम दूसरी ही बात कहने जा रहे हैं। उनसे कहेंगे कि ‘प्रदेश बचाओ और सरकार बनाओ’। लेकिन मैंने कार्यकर्ताओं को वचन दिया है कि ‘आप मुझे गंगा दीजिए, मैं आपको सत्ता दूंगी।’ मैं पूरी कोशिश करुंगी कि गंगा के कामों में भाजपा के कार्यकर्ता लगें और जनता को भी इसके लिए प्रेरित करें।
सवाल: आपने पार्टी से बाहर रहने के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को समान दूरी से देखा है। इनमें आपने क्या बदलाव देखा ?जवाब: जब हम राजनीतिक समीक्षा कर रहे होते हैं तो कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना होता है। यदि हमें अपने दल के बारे में कुछ कहना है तो हम दल के अंदर ही कहेंगे। मुझे ‘भारतीय जनशक्ति पार्टी’ में कभी कोई कमी दिखती थी तो मैं बाहर बोलने नहीं जाती थी। पार्टी के अंदर ही बैठकर बात होती थी। इसलिए जब मैं भाजपा की समीक्षा करूंगी तो पार्टी के अंदर बैठकर ही करूंगी। बाहर मीडिया के सामने तो नहीं ही करूंगी।
हां, जहां तक पूरी राजनीतिक व्यवस्था की समीक्षा का सवाल है तो मैं यह कह सकती हूं कि अभी एक समय आया है, जिसमें अचानक विचारधाराओं की अतिवादिता खत्म हुई है। जब देवगौड़ा की सरकार बनी तो उस समय वामपंथियों ने अपने आग्रह छोड़े। अपनी विचारनिष्ठाओं से कहीं न कहीं समझौता किया। फिर हमारी सरकार बनी, पर 2004 में हम नहीं जीत पाए। फिर मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो उसे बचाने का प्रयास हुआ। इस प्रयास में जो स्थितियां बनीं, उनसब को मिलाकर एक बात कह सकती हूं कि राजनीति में विचारनिष्ठा के पुनर्जागरण का युग आया है। फिर से उसको पुनर्स्थापित करना है।